अस्सी के दशक का वह वो दौर था जब श्रीदेवी का उदय हुआ ही था और जीतेंद्र के साथ उनकी फ़िल्मों का क्रेज़ था. फ़िल्म तोहफ़ा रिलीज़ होने से पहले ही हिट मानी जा रही थी. रंग-बिरंगे मटकों के बीच नाचती श्रीदेवी और जीतेंद्र का गाना ‘तोहफ़ा… तोहफ़ा’.. आने वाले कितने सालों के लिए मनोरंजक
अस्सी के दशक का वह वो दौर था जब श्रीदेवी का उदय हुआ ही था और जीतेंद्र के साथ उनकी फ़िल्मों का क्रेज़ था. फ़िल्म तोहफ़ा रिलीज़ होने से पहले ही हिट मानी जा रही थी. रंग-बिरंगे मटकों के बीच नाचती श्रीदेवी और जीतेंद्र का गाना ‘तोहफ़ा… तोहफ़ा’.. आने वाले कितने सालों के लिए मनोरंजक सिनेमा का मॉडल बन गया. हालात कुछ यूँ थे कि एक नए निर्देशक कुंदन शाह की फ़िल्म ‘जाने भी दो यारो’ भी तोहफ़ा के साथ ही रिलीज़ होने वाली थी. बाज़ार में न तो कुंदन शाह को कोई जानता था, न ही उनकी फ़िल्म की कास्ट को, सिवाय नसीरुद्दीन शाह के, और कुछ हद तक ओम पुरी के, लेकिन इस साल अक्तूबर में जब कुंदन शाह की 75वीं वर्षगाँठ मनाई गई, तो यक़ीन करना मुश्किल रहा कि सात लाख से कम बजट में, अनजान एक्टरों के साथ बनी फ़िल्म ‘जाने भी दो यारो’ आज अपने-आप में कल्ट मानी जाती है.
फ़िल्म में काम करने वाले तकरीबन हर कलाकार ने आगे चलकर अपनी प्रतिभा का झंडा गाड़ा, चाहे वह नसीर, ओम पुरी, सतीश कौशिक, सतीश शाह या फिर पंकज कपूर रहे हों. यूँ तो भारत में कॉमेडी फ़िल्मों की भरमार है , लेकिन 1983 में रिलीज़ हुई ‘जाने भी दो यारो’ उन चंद हिंदी फ़िल्मों में शुमार है, जिसने सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य को आज़माया. फ़िल्म के बनने की कहानी अपने-आप में एक लंबा चौड़ा किस्सा है. ‘जाने भी दो यारो’ ऐसी फ़िल्म है जिसमें हीरो कोई भी नहीं.. अगर हैं तो हर ओर विलेन ही विलेन और उनका शिकार हुए लोग. कुंदन शाह पुणे एफ़टीआईआई से निकलकर फ़िल्म बनाने की चाह में थे. कहानी उनके हाथ तब लगी, जब एफ़टीआईआई के बाद हैदराबाद में संघर्ष कर रहे उनके कुछ साथियों ने कुंदन शाह को अपने फोटो स्टूडियो के अजीबोग़रीब तजुर्बे सुनाए. उन्हीं दिनों कुंदन शाह को रिचर्ड एटनबरो की फ़िल्म ‘गांधी’ के लिए काम करने का ऑफ़र आया और इसके लिए उन्हें एक लाख रुपए मिलने वाले थे, जो उस वक़्त की एक बड़ी रक़म रही लेकिन अपने दोस्त सईद मिर्ज़ा का सलाह पर कुंदन शाह ने फ़िल्म ‘गांधी’ छोड़कर अपनी फ़िल्म की स्क्रिप्ट पर समय लगाने का फ़ैसला किया. एक अप्रैल 1982 को एप्रल फूल के दिन स्क्रिप्ट रजिस्टर करवाई गई.
हालाँकि फ़िल्म में सरकारी भ्रष्टाचार पर ही सवाल उठाए गए हैं लेकिन इसके बावजूद नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएफ़डीसी) इसे फाइनेंस करने का फ़ैसला किया, लेकिन ये रकम सात लाख रुपए से भी कम थी जिसमें केवल नसीरुद्दीन शाह को ही 15 हज़ार रुपए मिले बाकी सबको तीन से पाँच हज़ार तक की ही फ़ीस मिल पाई थी. दिल्ली के एक थिएटर निर्देशक रंजीत कपूर ने फ़िल्म लिखने का ज़िम्मा उठाया और उनके घर में रहने वाले एक नए कलाकार सतीश कौशिक को भी उन्होंने साथ रख लिया. चूँकि पैसे की ज़बरदस्त कमी थी तो इस फ़िल्म के प्रोडक्शन में कुंदन के दोस्त सुधीर मिश्रा, विधु विनोद चोपड़ा और उनकी दिवंगत पत्नी रेणु सलूजा भी पूरी तरह जुट गए. अगर आपने ये फ़िल्म नहीं देखी तो ये दो आदर्शवादी युवा फोटोग्राफ़रों रवि बासवानी (सुधीर) और नसीरुद्दीन शाह ( विनोद) की कहानी है.
फ़ोटो खींचते-खींचते उन्हें शहर के सरकारी अधिकारियों, बिल्डिंग माफ़िया (बिल्डर पंकज कपूर और शराबी बिल्डर ओम पुरी) और मीडिया (एडिटर शोभा) के बीच की भ्रष्टाचारी सांठगांठ का पता चलता है. और अहम सूबूत है भ्रष्ट कमिश्नर डिमेलो (सतीश शाह) की लाश और इस लाश की सबको तलाश है, और यहीं से शुरु होता है कॉमेडी ऑफ़ एरर का सिलसिला. दरसअल, फ़िल्म जाने भी दो यारो में नसीर का नाम विनोद चोपड़ा के नाम पर और रवि बासवानी का नाम सुधीर मिश्रा के नाम पर ही रखा गया था. आगे चलकर ये दोनों नामी निर्देशक बने. शुरु से लेकर अंत तक ‘जाने भी दो यारो’ में व्यंग्य भरा हुआ है, कहीं दबा हुआ, कहीं खुलेआम. मज़े की बात ये है कि ये तंज़ सरकारी अमले और बिल्डरों पर ही नहीं, फ़िल्मकार कुंदन शाह ख़ुद पर भी करते हैं. फ़िल्म की शुरुआत में ही जब नसीर और रवि बासवानी अपने नए ब्यूटी फ़ोटो स्टूडियो का उद्घाटन करते हैं और कोई ग्राहक नहीं आता तो नसीर कहते हैं– “कुंदन शाह से भी तो ढाई हज़ार उधार लिए हुए हैं, वो कैसे चुकाएँगे!”
फ़िल्म की एक ख़ास बात ये है कि इसमें बहुत सारे सीन ऐसे हैं, जो काफ़ी बेतुके लग सकते हैं लेकिन जिस मज़े से इन्हें निभाया गया है, ये पागलपन एक ज़बरदस्त सामाजिक हास्य-व्यंग्य का रूप ले लेता है. फ़िल्म में सतीश शाह ( कमिश्नर डिमेलो) ने ज़्यादातर समय एक लाश बनकर बिताया है. किसी सामान्य फ़िल्म में इस किरदार की कोई ख़ास भूमिका नहीं होती लेकिन निर्देशक और फ़िल्म एडिटर रेणु सलूजा की एडिटिंग का कमाल है कि वो लाश भी एक ज़बरदस्त हास्य किरदार बनकर उभरती है. मसलन, एक सीन है जहाँ पहियों वाले एक कॉफिन में सड़क पर सतीश शाह की लाश पड़ी है और उस पर फूलों वाला एक गोल हार रखा है. कॉफ़िन को ओम पुरी की ऑस्टिन गाड़ी से धक्का लगता है तो वो गोल हार सतीश शाह का हाथो में आकर स्टीयरिंग व्हील जैसा लगने लगता है, नशे में धुत बिल्डर ओम पुरी पहियों वाले कॉफ़िन को स्पोटर्स कार समझकर उसकी मरम्मत करने लगते हैं.
एडिटिंग के दौरान ओम पुरी और सतीश शाह के क्लोज़-अप के बीच इस तरह की इंटरकटिंग की गई है मानो वाकई दोनों में बातचीत हो रही है. कागज़ पर या पढ़ने में ये सीन मामूली-सा लगता है लेकिन पर्दे पर सतीश शाह और ओम पुरी की कॉमिक टाइमिंग ग़ज़ब की है. सतीश शाह को उस वक़्त ‘फ़निएस्ट डेड बॉडी’ कहा गया था. आज के दौर में फ़िल्म की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ‘जाने भी दो यारो’ के मीम्स की सोशल मीडिया पर धूम है, ख़ास तौर पर महाभारत वाले सीन से जुड़े तो बहुत सारे मीम्स हैं. महाभारत वाला क्लाइमेक्स सीन इस फ़िल्म का सबसे बेहतरीन हिस्सा माना जाता है. जहाँ हर पात्र डिमेलो (सतीश शाह) की लाश हासिल करना चाहता है जो नसीर और रवि बासवानी के पास है.
सीन ये है कि एक दूसरे का पीछ करते हुए सारे किरादर एक नाटक में पहुँच जाते हैं जहाँ महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण वाला सीन चल रहा है. गफ़लत में डिमेलो की लाश को साड़ी पहनाकर द्रोपदी बना दिया जाता है और नसीरूद्दीन लाश को स्टेज से हटाना चाहते हैं. वो ख़ुद दुर्योधन बनकर स्टेज पर आकर बोलते हैं कि द्रौपदी जैसी सती को देखकर मैंने चीरहरण का आइडिया ड्रॉप कर दिया है तो मंच पर अफ़रा-तफ़री फैल जाती है. वहीं पर भीम बनकर बिल्डर ओम पुरी भी पहुँच जाता है और कहता है कि ‘ओए धृतराष्ट्र के पुत्तर द्रौपदी को वापस कर, वो अब मेरे साथ जाएगी. द्रोपदी तेरे अकेले की नहीं है, हम सब शेयरहोल्डर हैं.’ परेशान धृतराष्ट्र का डायलॉग कि ‘ये सब क्या हो रहा है’ या युधिष्ठिर का संवाद कि ‘शांत गदाधारी भीम शांत’ अब मीम बन चुके हैं.
ये लेखक की कैसी कल्पना होगी कि महाभारत की इस धमाचौकड़ी के बीच अकबर और सलीम भी मंच पर आ जाते हैं और धृतराष्ट्र बना पात्र कहता है कि ‘थिस इज टू मच. ये अकबर कहाँ से आ टपका’. ‘हम उनकी याद में एक दिन के लिए इस शहर के सारे गटर बंद कर देंगे’ फ़िल्म देश में फैले भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही पर व्यंग्य के ज़रिए प्रहार करती है, जैसे एक सीन है जहाँ मुंबई के कमिश्नर गटर पर अध्ययन करने के लिए सरकारी खर्च पर महीनों के लिए अमरीका जाते हैं. और बाद में उनकी हत्या हो जाती है तो उनकी श्रद्धांजलि सभा में एक अधिकारी का भाषण कुछ यूँ है, “डिमेलो साहब कहा करते थे किसी देश की उन्नति की पहचान किसी चीज़ से होती है वो है गटर, हम उनकी याद में एक दिन के लिए इस शहर के सारे गटर बंद कर देंगे. इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप पीने का पानी एक दिन पहले भर के रख लें.”
इस घटना के पीछे कुंदन शाह के साथ हुआ एक असली वाक़या है. इसका ज़िक्र ‘जाने भी दो यारो’ सीरियसली फ़नी सीन्स 1983′ नाम की किताब में लेखक जय अर्जुन सिंह ने किया है. कुंदन शाह ने अर्जुन सिंह को बताया था, “हमारी बिल्डिंग में गटर का पानी लीक होकर पीने के पानी के टैंक में आ रहा था. मैं परेशान होकर सरकारी दफ़्तर गया. बदले में अफ़सर ने मुझसे कहा, ‘तो क्या हुआ. बहुत से लोग यही पानी पीते हैं?’ दरअसल, गटर शहर की, देश की फेल हो चुकी व्यवस्था का प्रतीक है जिसे बड़ी चतुराई से लेखकों ने, निर्देशक ने इस फ़िल्म में इस्तेमाल किया है. फ़िल्म में कॉमेडी ज़रूर है लेकिन इसमें उठाए गए मुद्दे बेहद गंभीर हैं. फ़िल्म मनोरंजन करती है लेकिन बहुत ही करारे व्यंग्य के ज़रिए. इसमें मेनस्ट्रीम सिनेमा की तरह बड़े सितारे या बजट नहीं, पर ये आर्ट फिल्म भी नहीं है. इसमें कॉमेडी न फूहड़ है और न किसी के जेंडर या शारीरिक बनावट पर इसमें फ़ब्तियाँ हैं. ये सब इस फ़िल्म की ख़ूबी है.
फ़िल्म का एक सीन है जो किसी भी एंगल से तर्क और लॉजिक से कोसों दूर हैं. सीन ये है कि नसीरुद्दीन शाह एक डिटेक्टिव बनकर भ्रष्ट बिल्डरों के कमरे में जाते हैं, जहाँ बिल्डर पंकज कपूर का राइट हैंड मैन सतीश कौशिक भी है. नसीर उन्हें बताते हैं कि आपके लिए सीक्रेट कॉल है और कोड वर्ड है ‘एलबर्ट पिंटो को ग़ुस्सा क्यों आता है’, यह उन दिनो नसीर की हालिया रिलीज़ फिल्म का नाम था. अब सतीश कौशिक और नसीरुद्दीन शाह एक ही कमरे में दो लैंडलाइन फ़ोन से एक दूसरे से बात कर रहे हैं. एक वक़्त फ़ोन गिर जाते हैं और तारें उलझ जाती हैं तो दोनों एक दूसरे के फोन से एक दूसरे से पीठ लगाकर बात करते हैं. सतीश कौशिक शीशे में नसीर को अपने ही कमरे में देख भी लेते हैं पर बातचीत जारी रहती है. इस बेहद बेतुके से लगने वाले सीन में से भी ज़बरदस्त कॉमेडी निकल कर आती है.
हालांकि पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि इस सीन को लेकर नसीरुद्दीन शाह नाराज़ हो गए थे. नसीरुद्दीन जिस मेथड एक्टिंग स्कूल से आते थे वहाँ इस तरह की एक्टिंग की गुंजाइश नहीं थी. इस फ़िल्म से पहले नसीरुद्दीन शाह आर्ट सिनेमा के स्टार बन चुके थे और ओम पुरी की अर्धसत्य अभी रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन कॉमेडी में दोनों का ही दख़ल नहीं था. पर ‘जाने भी दो यारो’ में पहली बार दोनों का ये अंदाज़ देखने को मिला और यही वजह भी थी कि दोनों ने ये फ़िल्म करने के लिए हामी भरी, हालांकि ओम पुरी को बिल्कुल आख़िर में लिया गया था. इस फ़िल्म में तकरीबन सभी कलाकार तब नए थे या संघर्ष कर रहे थे. पर उन्होंने इस कॉमेडी को बहुत संजीदगी से निभाया. फ़िल्म में एनएफ़डीसी के पैसे लगे थे जो सरकार से जुड़ी संस्था थी और सोचकर हैरानी ज़रूर होती है कि उन्होंने इसे पास कैसे किया.
‘जाने भी दो यारो-सीरियसली फ़नी सीन्स 1983 में लिखा गया है, “एनएफ़डीसी ने 6.84 लाख रुपए दे दिए थे. उनकी कमेटी को लगा कि ये फ़िल्म समाज पर एक तीखी टिप्पणी है. हमारे काम में कोई दख़लअंदाज़ी नहीं की गई. बल्कि ऐसी कई जगहों पर हमेशा शूट करने की अनुमति दिलाई गई जहाँ शूट करना मुश्किल होता है.” फ़िल्म का ज्यादातर बेतुकापन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, लेकिन बहुत कुछ सेट पर भी जुड़ गया. मसलन, महाभारत वाले सीन में जब ओम पुरी अचानक कपड़े बदलकर भीम बनकर पहुँच जाते हैं तो उनका काले शेड वाला चश्मा तब भी लगा हुआ है. ये स्क्रिप्ट में नहीं था पर ओम पुरी ने डाला. ओम पुरी की जो पंजाबी टोन है, वो भी उनका ही सुझाव था, हालाँकि कुंदन शाह इससे सहमत नहीं थे. पैसों की कमी की वजह से शूटिंग के दौरान अलग ही तरह की ‘कॉमेडी’ होती थी, जिसके किस्से मशहूर हैं.
एक सीन है जहाँ बहुत सारी औरतें बुर्का पहन मजलिस में जा रही हैं. सीन ऐसा है कि ओम पुरी से लेकर नसीर तक पूरी कास्ट एक दूसरे से बचने के लिए बुर्क़ों में हैं, लेकिन ग़ौर से देखें तो हर औरत ने काली की जगह अलग-अलग रंग का बुर्क़ा पहना हुआ है. दरअसल, हुआ ये था कि उस सीन के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा आर्टिस्ट की ज़रूरत थी, चूँकि पैसे नहीं थे तो फ़िल्म यूनिट के लोगों को ही बुर्क़ा पहनाकर खड़ा कर दिया गया और सिनेमटोग्राफ़र बिनोद प्रधान शूट करने लगे, लेकिन जब उन्हें सहायक की ज़रूरत होती तो वो उसी भीड़ में से उसे बुलाते थे, लेकिन पहचानने में दिक़्क्त हो रही थी, इसलिए सबको अलग-अलग रंग दे दिए गए. फ़िल्म में जब सब कुछ घनचक्कर की तरह ही चल रहा होता है तो बतौर दर्शक इसे भी पचा ले जाता है.
फ़िल्म में युवा पवन मल्होत्रा ने बतौर प्रोडक्शन असिस्टेंट काम किया है जो बाद में नामी अभिनेता के रूप में जाने गए. एक सीन के लिए कुंदन शाह को दो कबूतरों की ज़रूरत थी. पवन ने दो कबूतरों का इंतज़ाम किया लेकिन वो जगह काफ़ी दूर थी और उनके पास पिंजरे के पैसे नहीं थे, और न ही टैक्सी के. तो वो थैले में कबूतरों को रखकर लोकल बस में आए जिसका ज़िक्र भी किताब में किया गया है. और तो और, फ़िल्म में जो कैमरा दिखता है कि वो नसीर का अपना निकॉन कैमरा था जो शूटिंग के दौरान गुम हो गया था. फ़िल्म में मैगज़ीन एडिटर का काम किया था मराठी अभिनेत्री भक्ति बर्वे ने, ये रोल पहले अपर्णा सेन को ऑफर किया गया था. फ़िल्मी किस्सों की बात करें तो किस्सा मशहूर है कि वो फ़िल्म की कहानी सुनने के दौरान सो गईं और फ़िल्म करने से मना कर दिया. मराठी थिएटर में भक्ति बर्वे बहुत बड़ा नाम थीं और शफ़ी ईनामदार उनके पति थे. शुरुआती दिनों में भक्ति बॉम्बे दूरदर्शन की मशहूर न्यूज़रीडर हुआ करती थीं. 1996 में शफ़ी ईनामदार की मौत के पाँच साल बाद एक सड़क दुर्घटना में 52 साल की भक्ति का भी निधन हो गया था.
करीब 40 बरस पहले रिलीज़ हुई इस फ़िल्म को आज कैसे याद किया जाता है? पिछले साल की बात है जब निर्देशक सुधीर मिश्रा ने ये सवाल ट्विटर पर पूछा था कि अगर ये फ़िल्म आज रिलीज़ होती तो क्रिटिक इसे कितने स्टार देते. दिव्या दत्ता समेत इस फ़िल्म के फैन्स ने तो इसे पाँच में से छह स्टार दिए लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई इस फ़िल्म को कल्ट मानता है. सुधीर मिश्रा के सवाल पर फ़िल्मकार मुनीष भारद्वाज ने लिखा था, “मुझे नहीं लगता कि ये फ़िल्म समय की कसौटी पर खरी उतरती है. ये किसी स्कूल स्किट की तरह लगती है. मैंने इसे दोबारा देखने की कोशिश की और 10 मिनट में ही थक गया. एक्टिंग ओवर द टॉप है. लेखनी साधारण और क्राफ्ट कच्चा है.” ये बात सही है कि बजट की कमी का असर फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू पर दिखता है. कहीं-कहीं कंटीन्यूटी की कमी है तो महाभारत वाला एक दृश्य में कुछ धुँधला-सा लगता है. हुआ ये था कि नेगेटिव रोशनी से एक्पोज़ हो गया जिस वजह से फॉग डस्ट जमा हो गई लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि फिर से शूट किया जा सके. जिस तरह का ह्यूमर और तंज इस फ़िल्म है और जो क्रिएटिव लिबर्टी इस फ़िल्म में ली गई है क्या आज के दौर में ऐसा कर पाना संभव है ? लेखक सिद्धार्थ भाटिया ने भी ‘द वायर’ के अपने लेख में ये सवाल उठाया है.
वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्रन श्रीनिवासन कहते हैं, “आज का राजनीतिक माहौल ऐसा है कि जाने भी दो यारो जैसे व्यंग्य को बनाने से पहले फ़िल्मकार सोचेंगे. एमेज़ॉन ने भी एक सटायर बनाया है जिसे वो रिलीज़ नहीं कर रहे क्योंकि देश में ऐसा माहौल नहीं है. जब जाने भी दो यारो आई थी तब माहौल थोड़ा-सा अलग था हालांकि फ़िल्म में राजनीतकि एंगल था. फ़िल्म में सतीश शाह का सीन है जहाँ वो द्रोपदी बने हैं. आप सोचिए कि आज के दौर में वो सीन करें तो कितना विरोध हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग तो सिर्फ़ विरोध करने के लिए ही बैठे रहते हैं. इस तरह की फ़िल्म बनना मुमकिन नहीं.” एक और कारण है कि क्यों जाने भी दो यारो जैसी फ़िल्म दोबारा आसानी से नहीं बन सकती और वो ये कि इस फ़िल्म में हुनरमंद लोगों की भरमार है. नसीर से लेकर सुधीर मिश्रा तक एक से बढ़कर एक कलाकारों ने पर्दे पर, और पर्दे के पीछे काम किया है. सबने मिलकर इस फ़िल्म को पिरोया. आज के दौर में उतने सारे टेलेंट को साथ लाकर काम करना मुश्किल होगा क्योंकि इस तरह की साझेदारी अब महँगा सौदा है.
फ़िल्म का अंत कुछ ऐसा है कि तमाम कोशिशों के बाद दोनों आदर्शवादी फ़ोटोग्राफ़र यानी नसीर और रवि बासवानी सारे सूबुत पुलिस को दे देते हैं. वो सम्मानित किए जाने के सपने देखते हैं और वहीं पास में ‘सत्यमेव जयते’ का बोर्ड भी दिखता है लेकिन सारे भ्रष्टाचारी मिलकर एक हो जाते हैं और आख़िरी सीन में नसीर और बासवानी क़ैदियों के कपड़ों में शहर की सड़क पर जा रहे हैं. लोगों की भीड़ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और दोनों का पसंदीदा गाना ‘हम होंगे कामयाब’ बजता है और दोनों गर्दन काटे जाने का इशारा करते हैं. राज कपूर ने बाद में जब ये फ़िल्म देखी तो उन्होंने ज़िक्र किया था कि उन्हें फ़िल्म का अंत पसंद नहीं आया. बहुत लोगों को लगा कि ये कॉमेडी होते हुए भी निराशावादी फ़िल्म थी, जबकि कइयों को इसलिए पसंद आई कि दोनों युवाओं ने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा.
रिलीज़ होने के बाद ये फ़िल्म बहुत बड़ी हिट साबित नहीं हुई लेकिन बाद में इसने एक कल्ट क्लासिक की जगह हासिल की. पत्रकार रामचंद्रन श्रीनिवासन कहते हैं, “फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तो फ़्लॉप थी. लेकिन फिर टीवी पर, दूसरे माध्यमों पर इसे इतनी बार देखा गया कि ये कल्ट फ़िल्म बन गई. बहुत बार कल्ट फ़िल्में पहली बार तो फ्लॉप हो जाती हैं. लेकिन बाद में लोगों के दिल में जगह बना लेती है. जैसे ‘मेरा नाम जोकर’ थी. अक्सर ऐसा होता है कि वो फ़िल्में जो नया रास्ता बनाती हैं वो ख़ुद थक जाती हैं और बाद में उस रास्ते पर जो चलते हैं वो हिट हो जाते हैं. ‘जाने भी दो यारो’ की ख़ूबी ये है कि इसमें एक तरह की सादगी थी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के किरदार थे.” फ़िल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और रवि बासवानी को फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड. विधु विनोद चोपड़ा ‘परिंदा’ जैसी फ़िल्म बनाकर आने वाले सालों में बड़े निर्देशक बन गए. सुधीर मिश्रा ने ‘धारावी’ और ‘हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी’ बनाई. पवन मल्होत्रा, सतीश कौशिक, पंकज कपूर और नीना गुप्ता की अभिनय क्षमता दुनिया ने आने वाले सालों में देखी. इस फ़िल्म से अनुपम खेर का भी डेब्यू होने वाला था डिस्को किलर के किरदार के रूप में जिसे हर कोई करना चाह रहा था, लेकिन वो रोल एडिटिंग के दौरान कट गया. रंजीत कपूर ने फ़िल्म के लिए एक गाना लिखा था , वो गाना तो फ़िल्म में लिया नहीं गया लेकिन इस गाने से बोल चुराकर फ़िल्म का नाम रख दिया गया- ‘जाने भी दो यारो’ जो आज एक जुमला बन गया है. (बीबीसी इंडिया की टीवी एडिटर वंदना की रिपोर्ट)


















































































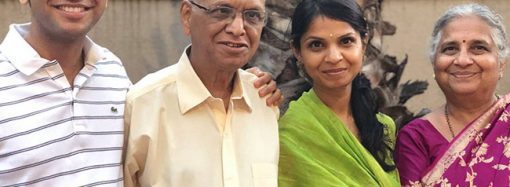



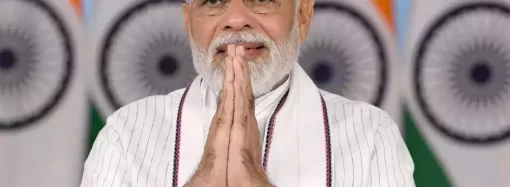
















































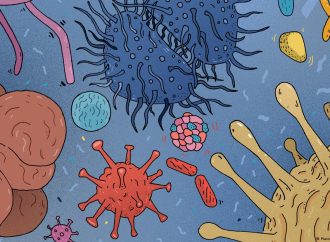


































































































Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *