अशोक पांडेय : जर्जर हो चुकने के बाद भी वह पुरानी साइकिल मट्टो पाल की जीवनरेखा है. कभी उसके पहिये का रिम टेढ़ा हो जाता है, कभी मडगार्ड उखड़ जाता है तो कभी उसकी धुरी का संतुलन बिगड़ने लगता है. मट्टो बेलदार है, दिहाड़ी पर मजूरी करता है. अक्सर बीमार पड़ जाने वाली बीवी से
अशोक पांडेय : जर्जर हो चुकने के बाद भी वह पुरानी साइकिल मट्टो पाल की जीवनरेखा है. कभी उसके पहिये का रिम टेढ़ा हो जाता है, कभी मडगार्ड उखड़ जाता है तो कभी उसकी धुरी का संतुलन बिगड़ने लगता है. मट्टो बेलदार है, दिहाड़ी पर मजूरी करता है. अक्सर बीमार पड़ जाने वाली बीवी से उसकी दो बेटियां हैं – नीरज और लिम्का. नीरज शादी के लायक हो गई है जिसके दहेज के लिए मट्टो से मोटरसाइकिल की मांग है. कायदे से किशोरवय लिम्का को स्कूल जाना चाहिए लेकिन ज़माने का चलन देखते हुए मट्टो ने उसे घर पर रखने का फ़ैसला किया हुआ है.
सूचना और चकाचौंध से अटी जो इक्कीसवीं शताब्दी हमें नज़र आती है, जंग लगी मट्टो की साइकिल उसकी छद्म आधुनिकता पर लगे असंख्य पैबन्दों को उघाड़ कर रख देती है. एक घटनाक्रम है. मट्टो सड़क किनारे टोकरी लगाए लौकी-तुरई बेच रहे अपने ही जैसे एक आदमी से मोलभाव कर रहा है. दूसरे किनारे पर झाड़ियों से टिका कर रखी गई साइकिल को वहां से गुज़र रहा एक ट्रैक्टर कुचल जाता है. इस त्रासदी के बाद दर्द और हताशा में किया गया मट्टो का दीर्घ आर्तनाद किसी क्लासिकल ग्रीक त्रासदी की याद दिलाता है. अगले दृश्य में चार लोगों का परिवार साइकिल की मृत देह के गिर्द बैठा शोक मना रहा है.
पिछली दफ़ा जब मट्टो के दोस्त कल्लू मैकेनिक ने साइकिल की मरम्मत की थी तो मट्टो ने उसमें नई घंटी लगवाई थी. कबाड़ी को तीन सौ रुपये में बेचे जाने से पहले घंटी को निकाल लिया जाता है जिस तरह मरे हुए लोगों की देहों से गहने निकाले जाते हैं. बाद में एक दिन छोटी बेटी लिम्का उस घंटी को बजाने का खेल खेल रही है. घंटी की यह आवाज़ मनुष्य के तौर पर हमारी सामूहिक पराजय के आख्यान को दर्ज करती जाती है और आप रोने लगते हैं.
पिछले महीने सितंबर में रिलीज़ हुई फिल्म ‘मट्टो की साइकिल’ में हमारे महादेश की दरिद्रता का एक ज़रूरी महाकाव्य रचा गया है. फ़िल्म आपको एक ऐसे संसार में लेकर जाती है, जो हमारी ऐन बगल में अस्तित्वमान है, पर अक्सर नज़र नहीं आता. इसके बावजूद कि दुनिया भर की सत्ताएं अपनी योजनाओं के केंद्र में इसी संसार को रखती हैं, सारी वास्तविक, ठोस और महत्वपूर्ण जगहों पर उसकी उपस्थिति ग़ायब है. सतत बड़ी होती गई इस अनुपस्थिति के लिए पूरी तरह हमारा मध्यवर्ग ज़िम्मेदार है, जिसने 1990 के बाज़ारवाद और वैश्वीकरण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और जो बड़ी बेशर्मी के साथ हर उस ताक़त के साथ खड़ा नज़र आता है जो इस दरिद्र संसार के जीवन को और ग़रीब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता.
मिसाल के तौर पर लगातार बड़े हो रहे गाड़ियों के चमकीले बाज़ार के दौर में इस बात की कल्पना तक नहीं की जा सकती कि लोग अब भी साइकिलें ख़रीदते होंगे. सच यह है कि साइकिलों की बिक्री लगातार बढ़ रही है. अखिल भारतीय साइकिल निर्माता संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि पहले कोरोना लॉकडाउन के बाद मई से सितंबर 2020 के दौरान कोई चालीस लाख साइकिलें बिकीं. यह संख्या इसी अवधि के पिछले वर्षों की तुलना में दो गुनी थी. देश की बहुसंख्य आबादी अब भी निर्धन है और उसके पास आने-जाने का यही सबसे सुलभ माध्यम है. यही उसकी हैसियत भी है.
इसी तरह गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे. उन पर चलने वाले लगातार हर तरह के संसाधनों को चूसते रहेंगे. साइकिल चलाने वाले अब भी बगैर नज़र आए उनके घर बनाने, बाथरूम ठीक करने, सड़कें चौड़ी करने और नालियां साफ़ करने जैसे हेय समझे जाने वाले काम करते रहेंगे. हर छोटे-बड़े नगर-कस्बे में सुबह आठ बजे लेबर चौकों पर उनकी मंडियां लगती रहेंगी, जहाँ सौ-पचास रुपयों के लिए उनके साथ जिरह होगी. दुनिया का काम चलता रहेगा. ‘मट्टो की साइकिल’ इसी क्रूर और असंवेदनशील दुनिया की तमाम नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ लिखी गई एक अर्जी है.
फ़िल्म के निर्देशक ने बगैर किसी जल्दबाज़ी के कहानी के परिवेश और उसकी डिटेलिंग पर मशक्कत की है जिसे उसके हरेक फ्रेम में देखा जा सकता है. मट्टो के घर की एक-एक चीज़ उसकी दरिद्रता की परिभाषा है. खुली नालियों वाले कच्चे रास्ते से लगी उसकी बाहरी दीवार पर लिखे नाम ‘इज्जत घर’ से लेकर भीतर धरीं मूंज की चारपाइयाँ, चूल्हा, बरतन, प्लास्टिक की ख़ाली बोतलें और खुला दालान जैसी चीज़ें इक्कीसवीं सदी की ग़रीबी का ऐसा सौंदर्यशास्त्र गढ़ती हैं जिससे आप, हम लगातार आँखें बचाते आए हैं.
एक एक्सप्रेस-वे का काम प्रस्तावित है, जो गाँव से होकर जाने वाला है. उसकी ज़द में आने वाली ज़मीनों के बदले में मिलने वाले मुआवजे ने वहां की युवा पीढ़ी के सपनों को पंख लगा दिए हैं जो किसी भी हाल में गाँव की ज़िंदगी जीना बर्दाश्त नहीं कर पा रही. लालच और अहंकार से परिभाषित होने वाली आज की राजनीति किसी बदसूरत विद्रूप की सूरत में समूची कथा के पार्श्व में पसरी पड़ी है जिसके भीतर ग्राम प्रधान और उसके गुर्गों के धृष्ट कारनामे हैं, उनकी बदकारियाँ है और लोलुपता का बजबजाता अंधा कुआं है.
मट्टो के पास नई साइकिल ख़रीदने को ढाई-तीन हज़ार नहीं हैं जबकि नया-नया प्रधान बना सिकन्दर चौधरी 27 लाख की नई गाड़ी ऐसे ही ख़रीद लाता है. मट्टो के जीवन में बहुत कम दुनियावी चीज़ों का दखल है और वह विकास और आधुनिकीकरण की दिशाहीन दौड़ में कहीं भी शामिल नहीं है. लेकिन दुनियावी चीज़ों से जब-जब उसका अपरिहार्य सामना होता है वह हर लड़ाई को हारता है. सभ्य समाज के पास उसकी निर्धनता के एवज़ में उसे देने को सिवाय हिकारत और घृणा के कुछ नहीं हैं. अस्पताल के डाक्टर से लेकर मोहल्ले में किराने की दुकान चलाने वाली बुढ़िया और थानेदार से लेकर साइकिल के दुकानदार तक किसी के पास न उसके जीवन को समझने की फुरसत है न संवेदनशीलता.
निर्देशक एम.गनी ने इस फ़िल्म में ढेर सारे रूपकों का इस्तेमाल किया है. इनमें से कुछ सायास हैं तो कुछ अनायास. मट्टो की साइकिल अक्सर बड़े मकानों के सामने या ऐसी जगहों पर बिगड़ती है जिनका निर्माण उसी के जैसे मशक्कत करने वाले हाथों ने किया होता है. साइकिल की मरम्मत करने वाले कल्लू मैकेनिक के यहां अक्सर बैठा रहने वाला पढ़ा लिखा वकील अख़बार में छपी खबरों का पारायण करने वाला एक ऐसा सामाजिक टिप्पणीकार है जो कभी स्वयं फ़िल्म का निर्देशक दिखाई देता है तो कभी एक तटस्थ सूत्रधार.
एक दृश्य में मट्टो की बड़ी बेटी नीरज किसी के खेत से एक कच्ची भिंडी तोड़ कर खा ही रही होती है कि खेत का मालिक आ जाता है. वह नीरज को डपटता ही नहीं उसकी ग़रीबी के बहाने उसके सारे परिवेश को चोर उचक्का बताता है. मौक़े पर वह नौजवान भी मौजूद है जो किसी ने किसी बहाने से बार-बार नीरज के पास पहुंचने की जुगत में रहता है. उसकी उपस्थिति भर से ही कहानी में एक अजीब सा सेक्सुअल तनाव निर्मित होने लगता है. जब नीरज को चोर बताया जा रहा होता है, वह ज़रा भी प्रतिवाद नहीं करता.
उसकी खामोशी नीरज को उसके सपनीले संसार से वास्तविकता में पटक देती है और वह क्रोध में जलती आँखों से साइकिल पर टहनियों का गठ्ठा लाद कर वहां से चली जाती है. उसे चोर कहने वाले किसान ने जो टी-शर्ट पहनी है उस पर अंग्रेज़ी में इबारत लिखी हुई है – ‘आई वॉज़ बॉर्न टू बी डिफरेंट नॉट परफेक्ट, सो डोन्ट जज मी.’ फ़िल्म के उत्तरार्ध में आप देखते हैं साइकिल के कबाड़ी के पास चले जाने के बाद उसका काम बाधित हो गया है. वह एक गहरे अवसाद में डूबता जाता है और उसकी अपनी हताशा शनैः शनैः उसके समूचे परिवार को चपेटे में ले लेती है.
नई साइकिल लेने के लिए ज़रूरी पैसे उसके पास नहीं हैं. यह निराश दौर खासा लंबा खिंचता है. बाजार में पटुवे की दुकान के लिए मालाओं में मोती पिरोने के काम से नीरज ने जो छह-सात सौ रुपये कमाए-बचाए हैं वह उन्हें अपने पिता को दे देती है. जैसे-तैसे अपने ठेकेदार की मदद से वह उधार में नई साइकिल ख़रीदता है. फ़िल्म की कहानी में जो दो चार अच्छे लोग दिखाई देते हैं वे कमोबेश मट्टो की जैसी ही आर्थिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं. मट्टो का ठेकेदार, कल्लू मैकेनिक, बेरोजगार वकील और मट्टो के साथी मजदूर.
ये मजदूर काम के बाद शाम को गाना गाते हुए घर लौटते हैं, ‘मोरा उतर गयो श्रृंगार भरे जोबन में’. हालांकि इनमें से किसी की भी कथा इस फिल्म में नहीं कही गयी है लेकिन तय है कि उनकी कहानियां भी मट्टो की कहानी जैसी ही हृदयविदारक होंगी. क्या विडम्बना है कि संसार में जो सबसे भले लोग हैं, उनके पास ज़रा भी उजाला नहीं बचा है जबकि सभ्यता के सबसे कमीने लोगों के पास उम्मीद और चौंध का अश्लील वैभव है.
काम से लौटते हुए एक दिन कुछ नकाबपोश बदमाश मट्टो की नई साइकिल लूट ले जाते हैं. बहुत थोड़े अंतराल पर घटी यह दूसरी त्रासदी मट्टो को बुरी तरह तोड़ कर रख देती है. साइकिल को वापस हासिल कर सकने की उसकी उम्मीदों का रास्ता व्यवस्था से होकर जाता है जिसकी एक-एक ईंट पर लोभ, मक्कारी और दुष्टता का वास है.
मट्टो की उम्मीदों के धीरे-धीरे टूटते जाने के साथ यह व्यवस्था क्रमशः नंगी होती चली जाती है और जब वह ग्राम प्रधान द्वारा दुत्कारे जाने के बाद पराजित क़दमों से वापस लौट रहा होता है, स्क्रीन के बीचों बीच एक दरिद्र इमारत पर लगा फहराता हुआ एक तिरंगा नज़र आता है. पार्श्व में ‘सारे जहाँ से अच्छा’ की करुण पुकार उभरती है. और हाथों में तिरंगे लिए कुछ स्कूली बच्चे मट्टो की उल्टी दिशा में दर्शकों की तरफ आते दिखाई देते हैं.
इस आख़िरी दृश्य से ठीक पहले प्रधान नई ख़रीदी गई अपनी सत्ताईस लाख की गाड़ी की पूजा करवा रहा होता है. मट्टो की साइकिल चोरी हो जाने को वह कोई तूल नहीं देता. उल्टे उसे दो कौड़ी की साइकिल का तमाशा बनाने की फटकार लगाता है. यह दृश्य अति-ड्रामाई होने के बावजूद स्मृति में गहरे अंकित हो जाता है और आप देर तक उदास होकर सोचते रहते हैं.
फ़िल्म में मट्टो की भूमिका प्रकाश झा ने निभाई है और कमाल का अभिनय किया है. हर दृश्य में वे वाक़ई मट्टो लगे हैं और उनकी ईमानदार आँखों को दयनीयता और उनकी देहभाषा देखने वालों को देर तक याद रहने वाली है. निर्धनता और बेबसी को विषय बनाकर बहुत सारी देशी विदेशी फ़िल्में बनी हैं लेकिन ‘मट्टो की साइकिल’ स्क्रीन पर रची गई एक ऐसी कलाकृति है जो आपको न सिर्फ़ आदमी बनने की तमीज़ सिखाती है, उसके भीतर ऐसे अनेक तत्व भी हैं जो आदमी को इक्कीसवीं सदी की आधुनिकता की सान पर परंपरागत सामाजिकता की परख करना सिखाते हैं.
तेज़ रफ़्तार फ़िल्मों के इस दौर में कई जगह यह फ़िल्म घिसटती नज़र आ सकती है. कई बार ऐसा भी लग सकता है कि एक ही जैसे दृश्यों को फ़िल्म में बार-बार क्यों दिखाया जा रहा है. जिस दुनिया में फ़िल्म का निर्देशक आपको ले जा रहा है वह दरअसल ऐसी ही है, धीमी, बोझिल और रोज़मर्रा चीज़ों से भरी हुई. फ़िल्म के आख़िरी हिस्से के आने तक रात में दीवार से लगी पुरानी साइकिल को देखता बीड़ी फूंकता विचारमग्न मट्टो फ़िल्म का ऐसा प्रतिनिधि रूपक बन जाता है, जिसके भीतर इस देश का मध्यवर्ग अपने को आईने में देखता हुआ पा सकता है. संवेदनशील हुआ तो वह अपनी कारगुजारियों पर शर्मिन्दा भी हो सकता है जिसके चलते देश के चप्पे-चप्पे पर बिखरे-छितरे मट्टो के जैसे अनगिनत त्रासद जीवन समाज और तथाकथित विकास की मुख्यधारा में दिखाई देना ही बंद हो गए या बंद करा दिए गए.


















































































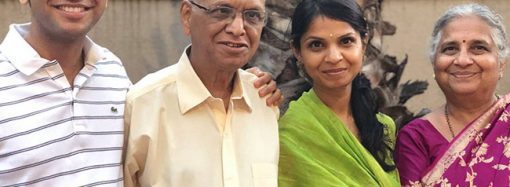



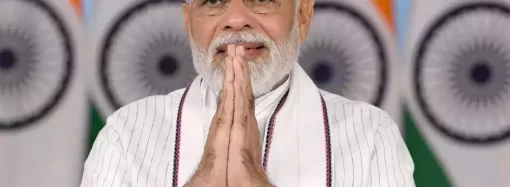
















































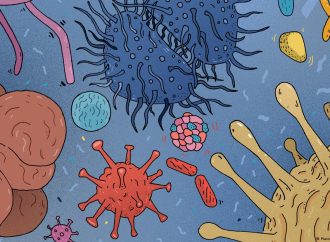


































































































Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *