अशोक वाजपेयी : नया वर्ष इस संदेह से शुरू हुआ कि शायद हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें नए विचार होना बंद हो गया है. लोकतंत्र के रूप में हमारी नियति अब भीषण संदेह के घेरे में है. राजनीति नागरिकों के बस में नहीं रही है- उनकी नागरिकता सिर्फ़ मतदान में बदल
अशोक वाजपेयी : नया वर्ष इस संदेह से शुरू हुआ कि शायद हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें नए विचार होना बंद हो गया है. लोकतंत्र के रूप में हमारी नियति अब भीषण संदेह के घेरे में है. राजनीति नागरिकों के बस में नहीं रही है- उनकी नागरिकता सिर्फ़ मतदान में बदल चुकी है. दिसंबर का आखिरी सप्ताह ग़ालिब के जन्मदिन का भी सप्ताह है. पर वही एक कारण नहीं है, ग़ालिब के यहां एक बार फिर जाने का. मैं दो कवियों के यहां बार-बार जाता हूं रिल्के और ग़ालिब. फ़ैज़ का एक मिसरा उधार लेकर कहा सकता हूं: ‘आस उस दर से टूटती ही नहीं.’
कुछ महीने पहले मुझे ‘गांधी की मौजूदगी’ पर एक व्याख्यान देना था तो मैंने शुरू में ही ग़ालिब के चार शेर उद्धृत करते हुए यह आग्रह किया कि उन शेरों की पहली पंक्तियां भूल जाए, दूसरी पंक्तियां याद रखें. इस प्रक्रिया को इधर मैंने आगे बढ़ाया तो पाया कि बारहा उनके यहां पहली पंक्ति फ़ारसी में लगभग तत्सम होती है और दूसरी उर्दू में. दो उदाहरण देखिए:
ऐ परतवे-खुर्शीदे-जहां ताब इधर भी
साये की तरह हम पे अजब वक़्त पड़ा है.
जौहरे-तेग़-बचश्मए-दीगर-मालूम
हूं मैं वो सब्ज़, कि ज़हराब उगाता है मुझे
अक्सर ग़ालिब क्रियापद का इस्तेमाल दूसरी पंक्ति में ही करते हैं, जो उर्दू में होता है. यह तो हम सभी को पता है कि ग़ालिब की महत्वाकांक्षा फ़ारसी के एक बड़े शायर की तरह माने जाने की थी और उनका फ़ारसी में कलाम उनके उर्दू के कलाम से चार गुना है. उनकी उर्दू शायरी में इसलिए फ़ारसी का गहरा प्रभाव होना लगभग लाज़िमी है.
बहरहाल मैंने बैठे-बैठे उनके शेरों की दूसरी पंक्तियों का एक छोटा-सा चयन तैयार किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन दूसरी पंक्तियों को सूक्ति की तरह, अपने संदर्भ से मुक्त, बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है. उनमें से कुछ का आम लोगों द्वारा होता भी रहा है. चयन इस प्रकार है:
इक ज़रा छेड़िए, फिर देखिए क्या होता है.
अब्र क्या चीज़ है? हवा क्या है?
दिल भी या रब कई दिए होते.
ज्यों चराग़ाने-दिवाली सफ ब सफ़ जलता हूं मैं.
वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूं मैं.
अब, अंदलीब, चल, कि चले दिन बहार के.
गोशे में कफ़स के, मुझे आराम बहुत है.
रहने दे अभी यां, कि अभी काम बहुत है.
दिया करते थे तुम तक़रीर, हम ख़ामोश रहते थे.
किसके घर जाएगा सैलाबे-बला मेरे बाद?
शाइर तो अच्छा है, प बदनाम बहुत है.
न हो जब दिल ही सीने में, तो फिर मुंह में जुबां क्यों हो?
गिरी है जिस पे कल बिजली, वह मेरा आशियां क्यों हो?
कुछ और चाहिए वुसअत, मिरे बयांं के लिए .
हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आस्मां क्यों हो?
तिरे बेमेहर कहने से, वह तुझ पर मेहरबां क्यों हो?
हज़र करो मिरे दिल से, कि इसमें आग दबी है.
देखना इन बस्तियों को तुम, कि वीरां हो गईं.
हर इक से पूछता हूं कि जाऊं किधर को मैं.
आता है, अभी देखिए, क्या-क्या, मिरे आगे.
दुश्मन भी जिसको देख के ग़मनाक हो गए.
वह समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है.
इक बिरहमन ने कहा है, कि यह साल अच्छा है.
दिल के खुश रखने को, ग़ालिब, यह ख़याल अच्छा है.
यां तक मिटे, कि आप हम अपनी क़सम हुए.
तेरे सिवा भी, हम पर बहुत से सितम हुए.
गर नहीं हैं, मिरे अशआर मैं मानी, न सही.
कि ताक़त उड़ गई, उड़ने से पहले, मेरे शहपर की .
इक शम्’अ रह गई है, सो वह भी ख़ामोश है.
मुझको को भी पूछते रहो, तो क्या गुनाह हो?
मरे बुतखाने में, तो का’बे में गाड़ो बिरहमन को.
बैठे हैं रहगुज़र पै हम, कोई हमें उठाए क्यों?
जिसको हो दीन-ओ-दिल अजीज़, उसकी गली में जाए क्यों?
राह में हम मिलें कहां, बज़्म में वह बुलाए क्यों?
लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार भी नहीं.
मौत से पहले आदमी, ग़म से निजात पाए क्यों?
जी में कहते हैं, कि मुफ़्त आए तो माल अच्छा है.
हम नहीं जलते, नफ़स हरचंद आतशबार है.
हम समझे हुए हैं उसे, जिस भेस में जो आए.
रोइए ज़ार-ज़ार क्या, कीजिए हाय-हाय क्यों?
नया वर्ष इस संदेह से शुरू हुआ कि शायद हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें नए विचार होना बंद हो गया है. लोकतंत्र के रूप में हमारी नियति अब भीषण संदेह के घेरे में है. राजनीति नागरिकों के बस में नहीं रही है- उनकी नागरिकता सिर्फ़ मतदान में बदल चुकी है. हर दिन उदार चित्त का एक स्तंभ धराशायी हो रहा है. करोड़ों लोग अपने धर्म-जाति-लिंग के कारण सार्वजनिक जीवन से ओझल हो रहे हैं. तरह-तरह के भय व्याप रहे हैं लेकिन अपराधी-दुष्कर्मी-भ्रष्ट-घृणा-उत्पादक आदि निर्भय घूम रहे हैं.
क्या इस भयावह स्थिति से निपटने बल्कि ठीक से समझने के लिए हमारी अब तक की वैचारिक संपदा नाकाफ़ी साबित हो रही है? क्या लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समता, न्याय, उदार समावेशिता, साझेदारी, परस्परता, बहुलता आदि के विचार अब अप्रासंगिक हो रहे हैं?
हमें कुछ नए वैचारिक औजार चाहिए जो हमें इस विकराल संकट को समझने, उससे उबरने, उसे बदल सकने में हमारे काम आएं. जिस तरह का ख़ालीपन व्याप गया है और जिस तरह की वैचारिक निष्क्रियता दृश्य पर छा गई है उनसे लगता है कि यह ज़रूरी कोशिश करने से हम ज़्यादातर कतरा रहे हैं. यह ख़ालीपन एक तरह का नया अकेलापन भी उपजा रहा है और शायद कहीं न कहीं हम इस अकेलेपन को अपना रहे हैं, वह हमें सुरक्षित लगता है और वेध्य होने की झंझट से बचा लेगा.
एक वृत्ति यह भी है कि हमें सारी भयावहता के बावजूद कोई जल्दी नहीं है और देर-सबेर हम कोई न कोई वैचारिक जुगाड़ कर लेंगे जैसे कि हम अपनी सुविधाजीविता में अब तक करते भी आए हैं. शायद हमारे कर्म और बुद्धि दोनों के भूगोल में विचारों की जगह नई चीजें, नई हिकमतें, नई टेक्नॉलजी आदि से हथिया ली है. नया वर्ष हमारे लिए वैचारिक धुंध से शुरू हुआ है.






















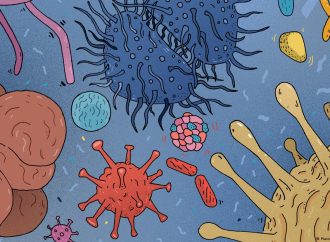























Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *