रामजनम पाठक : अक्तूबर या शायद नवंबर 1995 या 96 की एक धुंधुआती शाम को जब अपना माल-असबाब एक ट्रक में समेट कर मैं इलाहाबाद से बरेली के लिए निकला था तो कुछ-कुछ ” बेआबरू होकर कूचे से निकले” जैसा ही महसूस किया था। मैं इलाहाबाद छोड़कर कतई कहीं जाना नहीं चाहता था। जब हमारा
रामजनम पाठक : अक्तूबर या शायद नवंबर 1995 या 96 की एक धुंधुआती शाम को जब अपना माल-असबाब एक ट्रक में समेट कर मैं इलाहाबाद से बरेली के लिए निकला था तो कुछ-कुछ ” बेआबरू होकर कूचे से निकले” जैसा ही महसूस किया था। मैं इलाहाबाद छोड़कर कतई कहीं जाना नहीं चाहता था। जब हमारा ट्रक फाफामऊ पुल पार कर रहा था तो मैंने छूटते इलाहाबाद को इतने कातर भाव से देखा कि मेरी आंखों की कोरों में पानी भर गया। गंगा की पतली धार मुझे ठीक से दिखी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बलात् अपहरण किया जा रहा है। मुझे तुलसीदास के सीताजी की याद आई,’जिमि म्लेच्छ बस कपिला गई। ‘
ऐसा नहीं था कि इलाहाबाद में बहुत सुरक्षा थी या कोई पक्का ठौर-ठिकाना था या पक्की नौकरी थी। बल्कि, इसका उलटा ही था। अर्द्ध-बेकारी थी, अनिश्चितता थी, आवारगी थी। जिसे निश्चिंतता कहते हैं और जिन कारणों से लोग बाहर निकलने के जोखिम से ठिठकते हैं, वैसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ। यह जोखिम तो मैं बस्ती से निकलते समय ही उठा चुका था। दस-बारह साल यहां बिताने के बाद मैं अब एक और जोखिम लेने से डर रहा था। अनजानी दुनिया में जाने का जो भय होता है, वह मुझे आपादमस्तक घेरे हुए था। क्या सिर्फ इतनी ही बात थी। बहुत गंभीरता से मैंने सोचा इस बारे में। आखिर, इलाहाबाद से लगाव की इतनी गहरी वजह क्या थी ? क्या इसलिए कि दस-बारह साल यहां रहा था या यहीं शादी हो गई थी या साहित्यकारों-कलाकारों की मंडली को मैं छोड़ना नहीं चाहता था या कुछ गाढ़े के मीत थे यहां। नहीं, यहां का साहित्यिक परिदृश्य मुझे दोनों बांहों से जकड़े हुए थे। यों यहां रहते हुए मुझे इसका एहसास नहीं था। गेट बाहर होते ही इस ऐतिहासिक शहर की महत्ता और महिमा मेरी समझ में आ गई।
इलाहाबाद मेरे अवचेतन में समाया हुआ है। मेरी कविताओं में, और कहानियों में भी, इलाहाबाद बार-बार आता है। दो भागों में लिखी मेरी एक कविता का शीर्षक ही है-‘तुम मेरा घोंसला हो इलाहाबाद।’ समालोचक सुधीश पचौरी ने मेरी कविताओं की भूमिका लिखते हुए उन्हें ”इलाहाबादी ठाठ की कविताएं” कहा है। यह जो जकड़न है, ये जो अदृश्य जंजीरें हैं, यह जो कहीं रम जाने का भावबोध है, वही तुम्हारा बाहुपाश है। जब कोई शहर ही तुम्हारी प्रेमिका बन जाए तो कवि पुकार उठता है- रुपसि, तेरा घन केशपाश! यही वह केशपाश है, जो तुम्हें तार-तार, क्षार-क्षार कर देता है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी आलोड़न-विलोड़न है, कुछ भी उठा-पटक है और तुम कुछ भी कर गुजरना चाहते हो तो तुम्हें अपने मतलब का, अपने लायक, अपने मनमुताबिक जगह चाहिए ही चाहिए। मुक्तिबोध का ‘अंधेरे में’ का वाचक पूछता है–कहां जाऊं, दिल्ली या उज्जैन ?
बरेली में ईसाइयों की पुलिया में जाकर मैंने बड़ा-सा मकान ले लिया। अपनी औकात से ज्यादा। काहे कि इलाहाबाद में मैं हमेशा एक कक्षीय-सदन में रहा था। तो बड़ी हसरत थी खुल्ले में रहने की। यहां तक कि मेरी शादी हुई तो पत्नी विदा होकर उसी एक कक्षीय-प्रासाद में आईं। मैं अपने दारिद्रय और अल्पवेतनभोगिता पर लाजों मर-मर जाता था। बनिस्बतन, बरेली में सब कुछ ठीक था। मगर ईसाइयों की पुलिया के बगल में ट्रकों की ऐसी रेलमपेल रहती कि अहर्निश धूल-धुक्कड़ का उत्पादन होता रहता और अंगने में जो कपड़े सूखने को डाले जाते, वे काले-चीकट हो जाते। मेरा कार्यालय भी ऐसी जगह था, जहां गोबरों की दुर्गंध से पटा-पड़ा मैदान सबसे पहले आपका स्वागत करता। वहीं कोने में एक चाय-समोसे की दुकान थी, जहां रात में मैले-कुचैले लोगों का जमावड़ा रहता। कहां इलाहाबाद की साफ-सुधरी दुकानें और कहां श्यामतगंज की वह नाले पर टंगी बदबूदार झोपड़ी। मगर झोपड़ी का माहौल जितना दमघोंटू था, उससे ज्यादा दफ्तर का था। कोई सखा, न संगी। मुझे औदास्य और अवसाद ने अपने घेरे में ले लिया। इलाहाबाद में अखबारों के दफ्तर इतने संकुचित, कसे हुए और सामंती नहीं थे, जितना मैंने बरेली और मुरादाबाद में देखा। ‘अमृत प्रभात’ जैसे अखबार का खुला दफ्तर मैंने फिर कहीं नहीं देखा। दफ्तरों का भी अपना एक व्यक्तित्व होता है। उनकी कद-काठी और रचाव-सिंगार देखकर आप समझ सकते हैं कि उनमें धड़कन है या नहीं या बस मुर्दा दीवारों से घिर से हैं आप।
इलाहाबाद के दफ्तरों में बाउंसर टाइप के गार्ड नहीं होते थे, वहां विज्ञप्तिदाता रिपोर्टिंग रूम तक आते थे और इस बहाने अपने रिपोर्टरों से भी मिल लेते थे। रिपोर्टरों की अपने लोगों से जान-पहचान हो जाती था। अब मै, जहां आ गया था, इन शहरों में नागरिकों, पाठकों की गेट से अंदर जाने पर मनाही थी। बाद में, दिल्ली में हालत और खराब देखी। दफ्तरों के बाहर गार्ड ऐसे बंदूक लिए तैनात रहते हैं, मानो अंदर कोई जालसाजी चल रही हो। अखबारों के संपादकों, यूनिट संपादकों और डेस्क प्रभारियों की कभी चर्चा करूंगा। एक प्रसंग जरूरी है। हुआ यह कि मुझे जब नियुक्तिपत्र मिला तो मैंने अखबार के मालिकनुमा निदेशक को सोचा कि धन्यवाद कह दूं। उस समय तो वे कुछ नहीं बोले। बाद में किसी अन्य प्रसंग में उन्होंने कहा, ‘ आप बातचीत में बहुत याराना हो जाते हैं। आप तो इलाहाबाद से आए हैं, आपको ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक होना चाहिए।”
मैं समझ गया कि वे क्या चाहते हैं। जो लोग सोचते हैं कि देश-दुनिया से दास -प्रथा खत्म हो गई है, उन्हें अखबारों के दफ्तरों का सर्वेक्षण करना चाहिए। भाषाई और कस्बाई पत्रकारिता में मालिकों से लेकर संपादकों और प्रभारियों के पैर छूने का चलन निश्चय ही विद्यानिवास मिश्र ने नहीं शुरू किया होगा। यह अखबारों के दफ्तरों में व्याप्त असुरक्षाबोध, अयोग्यता, अल्पशिक्षा और मालिकों की सामंतशाही का नतीजा है। लालच, भय और स्वाभिमान की कमी लोगों को लाचार कर देती है कि वे आगे बढ़ने के लिए कोई गैरजरिया तलाश लेते हैं। मेरी हालत आसमान से गिरे खजूर पर लटके वाली थी। इलाहाबाद वापस नहीं हो सकता था। जिय संशय कुछ फिरती बारा। मैं लड़- झगड़कर तीन महीने में मुरादाबाद जा पहुंचा। उसी मुरादाबाद में जो मुल्ला और मच्छर के लिए बदनाम तो पीतल और जिगर मुरादाबादी के लिए सन्नाम था।
मुरादाबाद ने मुझे काम दिया और नाम भी। यहीं मशहूर फिल्मकार सागर सरहदी मुंबई से चलकर मेरी कहानी पर फिल्म बनाने के लिए कांट्रेक्ट साइन कराने आए। जब मैंने स्टेशन पर उन्हें विदा किया तो बोले,-‘खाओ, पियो, चाय पियो, शराब पियो मगर पढ़ो खूब।’ मैंने पूछा पढ़ने से क्या होगा। बोले,”-पढ़ने से रूह बेखौफ होती है।” मैं दंग रह गया। मैंने सुना कि उनके पास बीस लाख रुपए से ज्यादा की किताबें थीं। मैंने इस बात को गांठ बांध ली। मैंने अपनी रूह को कभी खौफजदा नहीं होने दिया। डरता हूं, मगर नहीं डरता।
बस, इस बात से डरता हूं कि किसी का अनभला न हो जाए। कहीं शेर पढ़ा था–लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं। इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। अच्छा हुआ, इलाहाबाद से निकल आया। नहीं तो पता नहीं क्या होता। सुना है कि अब साहित्यिक विमर्श, विचारों की उठापटक, मनीषियों की जमघट उठ चुकी है। काफी हाउस, माधुरी मिष्ठान्न भंडार, एजी आफिस की ‘संसद’ की बैठकें बीते दिनों की बातें हैं। दो ऐतिहासिक कांग्रेसी परिवार सत्ताधारी दल की चपेट में है। समय ही नहीं बदला है, लोग भी बहुत बदल गए हैं।


















































































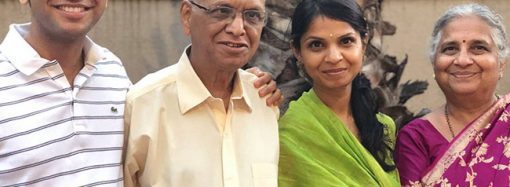



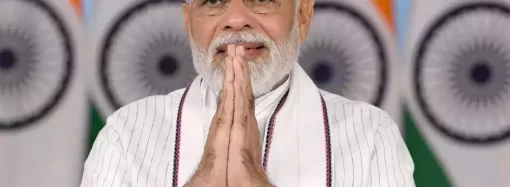
















































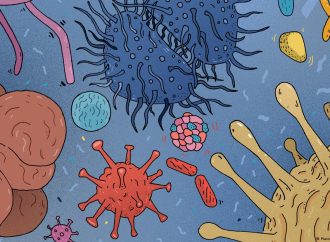


































































































Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *