भावना जुयाल : वेशभूषा से किसी भी इलाके के स्थानीय निवासियों की पहचान होती है. ये वेशभूषाएं पारंपरिक तौर पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहनी जाती हैं. ये पारंपरिक परिधान औए वेशभूषाएं कैसी होंगी यह कई बातों से तय होता है मसलन क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु, निवासियों की जीवन पद्धति, निर्माण सामग्री की उपलब्धता, आर्थिक सम्पन्नता,
भावना जुयाल : वेशभूषा से किसी भी इलाके के स्थानीय निवासियों की पहचान होती है. ये वेशभूषाएं पारंपरिक तौर पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहनी जाती हैं. ये पारंपरिक परिधान औए वेशभूषाएं कैसी होंगी यह कई बातों से तय होता है मसलन क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु, निवासियों की जीवन पद्धति, निर्माण सामग्री की उपलब्धता, आर्थिक सम्पन्नता, रहन-सहन इत्यादि. सामान्यतः उत्तराखण्डी पुरुषों अथवा महिलाओं का परम्परागत परिधान लावा होता था. जाड़ों में यह एक कंबलनुमा ऊनी कपड़े से सिर से पैर तक ढंक लेने वाला एक परिधान होता था, जिसे सूई-संगल से बांधकर रखा जाता था. गर्मियों में सूती लावा (एक काली चादर) पहना जाता था. वक़्त बदला और पुरुषों के बीच इसकी जगह लंगोट और मिरजई ने ले ली.
उत्तराखण्ड के सीमान्त इलाके में साल के बारहों महीने ठण्ड हुआ करती है इसलिए यहां के लोग परिधानों के रूप में ऊनी कपड़ों का ज्यादा इस्तेमाल किया करते हैं. गरीब लोग स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों से ही वस्त्र बना लिया करते थे. भेड़ों की ऊन, जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल, कपास से निकलने वाली रूई या भांग के रेशों को कातकर कपड़े बनाये जाते थे. बुनियादी सुविधाओं तक से वंचित रहने वाले पहाड़ी महिला-पुरुषों की तरह ही यहां के बच्चों और शिशुओं के परिधान भी बहुत कम ही हुआ करते थे.
बालकों के लिए कुर्ता, सन्तरास, गतौड़ी, कनछोपी जैसी पोशाकें हुआ करती थी. कुछ अमीर घरों के बालक ही पजामा पहना करते थे. बालिकाओं के लिए तो केवल एक ही परिधान हुआ करता था— ‘झगुल’अथवा ’झगुली.’ इन्हीं के बारे में जानते हैं थोड़ा विस्तार से. पहाड़ों में मान्यता है कि नवजात शिशुओं को नामकरण से पहले नये सिले हुए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए. इसलिए किसी पुराने कपड़े को इस तरह काटा जाता था कि उसके बीच से शिशु के दोनों हाथ बाहर आ जाएं और उसका सीना ढंक जाए. पीछे से यह खुला रहता था. इस वस्त्र को गतोड़ी कहा जाता था.
उत्तराखण्ड के बाल परिधानों में ‘झगुली’ बालिकाओं का एकमात्र परिधान हुआ करता था. इसकी लम्बाई जरूरत से ज्यादा रखी जाती थी ताकि बढ़ते बच्चे के हिसाब से यह जल्दी छोटा न हो. क्योंकि गरीबी इतनी थी कि अक्सर नए कपड़े सिलवाना मुमकिन नहीं था. इसीलिए पुराने कपड़ों पर ही बार-बार टल्ले लगाकर उनका उपयोग किया जाता था. यह झगुली दिखने में आज की मैक्सी की तरह ही हुआ करती थी. इसके दो हिस्से हुआ करते थे, ऊपरी हिस्से में कमर से गर्दन तक खोलने-बन्द करने के लिए बटन लगे होते थे और निचले हिस्से में चुन्नटदार घेरा होता था. तब लोगों के पास दो-तीन जोड़ी ही कपड़े हुआ करते थे, उन्हें ही बदल-बदलकर पहना जाता था. तीज-त्यौहार, शादी-ब्याह के मौके पर एक नया झगुला बनाकर रख दिया जाता था और ऐसे हर मौके पर उसी को पहना जाता था.
पहाड़ों में लोगों की दिनचर्या इतनी व्यस्त होती थी कि उन्हें अपने बच्चों की देखभाल का समय ही नहीं मिलता था. इसलिए छोटे बच्चों को ऐसी ड्रेस पहना दी जाती थी जो सुविधाजनक भी हो और जब घर के बड़े खेतों या जंगल के कामों में व्यस्त हों तो बच्चों को मल-मूत्र त्याग में कोई कठिनाई न हो. बच्चों का यही कपड़ा कहा जाता था सन्तरास. इसकी सिलावट फौजियों की डांगरी की तरह होती थी, जो मल-मूत्रत्याग की सुविधा के लिए दोनों टांगों के बीच से खुली हुआ करती थी. पीठ की ओर से बन्द करने के लिए बटन या कपड़े की घुंडियां लगी होती थी.
कनछोपी/कनटोपी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह बालक-बालिकाओं या शिशुओं द्वारा सिर के ऊपर पहना जाता था. मोटे गरम कपड़े को इस तरह सिला जाता था कि वह सिर सहित दोनों कानों को अच्छे से ढँक ले. इसमें ऊपर से कान के नीचे तक आने वाले दोनों सिरों पर तनियां लगी होती थी, जिन्हें ठोड़ी के नीचे बांध दिया जाता था. सजावट के लिए पीछे की ओर से एक झालर सी भी लटका दी जाती थी. जाड़ों के दिनों में ठण्ड के प्रकोप से बचाये रखने के लिए इससे ज्यादा बेहतर परिधान नहीं हो सकता था.
गनौती को ठण्ड से होने वाली बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए, कूटे हुए अजवाइन, हल्दी, मेथी इत्यादि को एक खुले कपड़े की पतली-लम्बी थैली में भरने के बाद, सिलकर बनाया जाता था. जो दोनों ओर से संकरी और बीच में फैली हुई होती थी. इसके सिरों पर तनियां लगाकर शिशु के गर्दन पर बांध दिया जाता था. आधुनिक दौर ने महानगरों ही नहीं बल्कि सुदूर पहाड़ी गाँवों को भी तेजी से बदल दिया है. इस बदलते परिदृश्य में गाँव और यहां की संस्कृति, परम्पराएं, जीवनबोध, यहां तक कि मूल संवेदनाएं भी खोती जा रही हैं. परम्परागत परिधानों की जगह बाजार के रेडीमेड कपड़ों ने ले ली है. अपने परम्परागत वस्त्राभूषण, व्यंजन, स्थापत्य, वाद्ययंत्र, व्यवसाय इत्यादि सभी कुछ बीते समय की बातें होती जा रही हैं.


















































































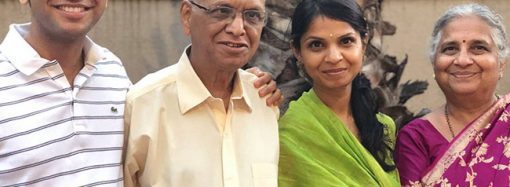



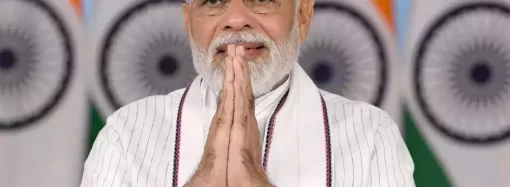















































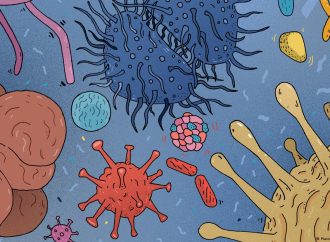



































































































Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *